उपसर्ग तथा प्रत्यय: अर्थ, परिभाषा, भेद, उदाहारण (Prefix and Suffix)
उपसर्ग तथा प्रत्यय (Prefix and Suffix) | का अर्थ, परिभाषा, भेद, और उदाहारण इस पोस्ट में बहुत अच्छे से समझाया गया है एक नजर जारूर देखे...
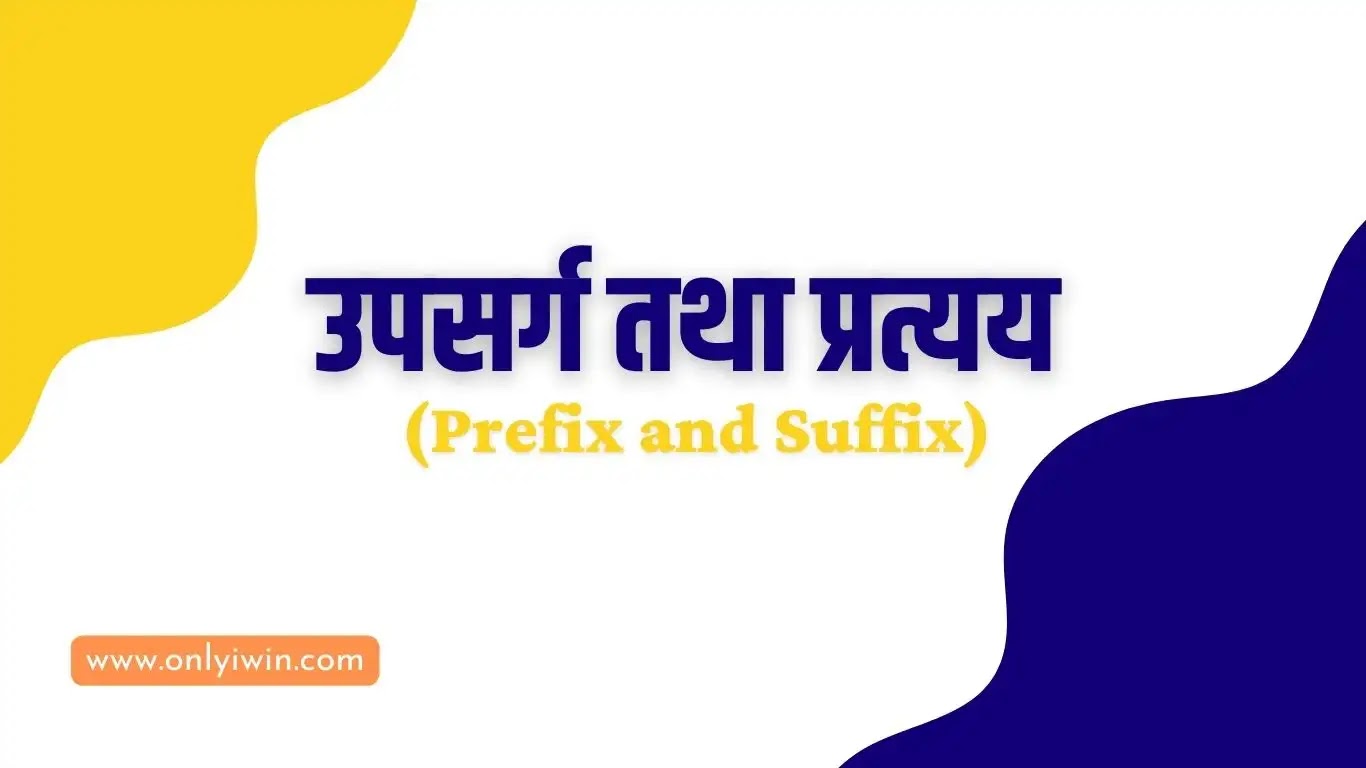 |
| उपसर्ग तथा प्रत्यय (Prefix and Suffix) |
उपसर्ग तथा प्रत्यय (Prefix and Suffix)
उपसर्ग तथा प्रत्यय शब्द की रचना कैसे करते है?
भाषाओं में शब्द कैसे बनते हैं? कभी आपने सोचा है? हर भाषा में नई-नई संकल्पनाओं के लिए नए-नए शब्द बनाए जाते हैं। भाषा में नई-नई संकल्पनाएँ आती रहती हैं और हम उनके लिए नए-नए शब्द बनाते रहते हैं। प्रत्येक भाषा में तीन तरह से शब्द बनाए जाते हैं -
1. मूल शब्द के आरंभ में कोई अंश (शब्द रूप) जोड़कर; जैसे
वि + योग = वियोग
बे + ईमान = बेईमान
अन् + आदर = अनादर
अ + सुंदर = असुंदर
नये शब्द बनाने के लिए मूल शब्द के आरंभ में जो अंश जोड़े जाते हैं, उन्हें उपसर्ग कहते हैं।
2. मूल शब्द के अंत में कोई अंश (शब्द रूप) जोड़कर, जैसे
ईमान + दार = ईमानदार
योग + ई = योगी
आदर + नीय = आदरणीय
सुंदर + ता = सुंदरता
मूल शब्द के अंत में जुड़नेवाले अंश को प्रत्यय कहते हैं।
3. दो मूल शब्दों को मिलाकर; जैसे
राष्ट्र + पिता = राष्ट्रपिता
ऋण + मुक्त = ऋणमुक्त
प्रधान + मंत्री = प्रधानमंत्री
काली + मिर्च = कालीमिर्च
दो शब्दों के मेल से बनने वाले नए शब्दों को समास या समस्तपद कहते हैं।
- उपसर्ग द्वारा
- प्रत्यय द्वारा
- समास द्वारा
उपसर्ग के कई नाम है जैसे- आदि प्रत्यय, व्युत्पत्तिमूलक प्रत्यय, रचनात्मक प्रत्यय
उपसर्ग की परिभाषा
वे शब्दांश, जो किसी शब्द के आरम्भ में लगकर उनके अर्थ में विशेषता ला देते हैं अथवा उसके अर्थ को बदल देते हैं, उपसर्ग कहलाते हैं।
शब्दों तथा उपसर्गो में यहीं अंतर होता है कि उपसर्ग शब्दों की तरह अर्थवान तो होते हैं, पर स्वतंत्र नहीं होते अर्थात इनका भाषा में प्रयोग अलग से स्वतंत्र रूप में नहीं हो सकता।
उपसगों से बने शब्दों के कुछ उदाहरण इस प्रकार है-
नि + युक्त = नियुक्त
अधि + नायक = अधिनायक
अव + मानना = अवमानना
उत् + नति = उन्नति
उपसर्ग: भेद प्रभेद
जिस तरह स्रोत के आधार पर शब्दों के तत्सम तद्भव तथा देशज तथा आगत के रूप में भेद किए जाते हैं, उसी तरह उपसर्गो के भी निम्नलिखित भेद किए जा सकते हैं-
- तत्सम उपसर्ग
- तद्भव उपसर्ग / हिंदी के उपसर्ग
- आगत / विदेशी उपसर्ग (अरबी-फारसी, अंग्रेजी के उपसर्ग)
तत्सम उपसर्ग
जो उपसर्ग तत्सम शब्दों के साथ संस्कृत भाषा से हिंदी में आ गए हैं तथा हिंदी के तत्सम शब्दों के ही प्रारंभ में जुड़कर शब्द बनाते है. वे तत्सम उपसर्ग कहलाते हैं। तत्सम उपसर्गों की संख्या 22 है जो इस प्रकार है-
- अति - बाहुल्य (अधिक, उस पार)
- अधि - सामीप्य, ऊपर, श्रेष्ठ
- अनु - पीछे, साथ, समान
- अप - दूर, हीनता, विरुद्ध
- अभि - ओर, सामीप्य
- अव - दूर, नीचे
- आ - तक, कम, इधर
- उत्, उद् - ऊपर, उन्नति
- उप- निकेट, सहायक, छोटा
- दुः दुर् - बुरा, कठिन
- दुश्, दुष्, दुस् -बुरा, कठिन
- नि- नीचे, भीतर
- निः निस् - बिना, बाहर, निषेध
- निर् - बिना, बाहर, निषेध
- परा - पीछे, उलटा
- परि - चारो ओर
- प्र - अधिक, आगे
- प्रति - ओर, उलटा, विरोध, प्रत्येक
- वि - बिना, अलग, विशेषता
- सम् - पूर्ण, अच्छी तरह, संयोग
- अन् - नहीं / बुरा
- सु- अच्छा, सुन्दर, सहज
तद्भव उपसर्ग / हिंदी के उपसर्ग
जिन उपसगों का विकास संस्कृत के तत्सम उपसर्गों या समासों के पूर्वपदों से हुआ है, वे तद्भव उपसर्ग कहलाते हैं। इन्हें हिंदी के उपसर्ग भी कहते हैं। इनमें कुछ उपसर्ग ऐसे होते हैं जो संस्कृत के मूल उपसर्गों के रूप में थोड़े-बहुत परिवर्तन के साथ विकसित हुए हैं; जैसे अधः 🠆 अध, कु 🠆 क. सु 🠆 स आदि।
कुछ संस्कृत के तत्सम् उपसर्ग हिंदी में आकर हिंदी के अपने बन गए तो यथावत रूप में तद्भव शब्दों के साथ लगकर शब्द रचना करने लगे। अतः आपको कुछ उपसर्ग जो तत्सम उपसर्गो की सूची में मिलते हैं. वे तद्भव या हिंदी उपसगों की सूची में भी दिखाई देंगे, परंतु तद्भव उपसर्ग के रूप में ये तद्भव शब्दों के साथ मिलकर नए शब्दों की रचना करेंगे, यह ध्यान रखिए।
हिंदी में उपसर्ग 10 होते है -
- अ-अन- रोकना, मना करना
- अध - आधे, अपूर्ण
- ऊन - एक कम
- औ (अव) - मना करना
- दु - हीन, बुरा
- नि - अभाव, विशेष, निषेध
- बिन - निषेध
- भर- ठीक, पूरा
- कु (क) - बुरा, हीन
- सु (स) - श्रेष्ठ साथ
विशेष टिप्पणी: हिंदी में कुछ व्याकरण लेखक 'क' और 'स' क्रमशः नवें और दसवें (कु एवं के विकार) को अलग मान कुल बारह उपसर्ग बताते हैं, परन्तु इन दोनों को अलग उपसर्ग नहीं माना जाना चाहिए।
आगत विदेशी उपसर्ग
विदेशी भाषाओं से जो उपसर्ग हिंदी में आ गए हैं, उन्हें आगत उपसर्ग कहते हैं। इनमें उर्दू, अरबी-फारसी, ओखी आदि भाषाओं से आने वाले उपसर्ग आते हैं।
उर्दू उपसर्ग-(19)
- अल (अरबी) - निश्चित
- ऐन - ठीक, पूरा
- कम - थोड़ा, हीन
- खुश - अच्छा, शुभ
- गैर - भिन्न, विरुद्ध
- दर - में
- ना - अभाव
- फ़िल् - में फी (अरबी) में प्रति
- ब - अनुसार, में, से ओर
- बद - बुरा, अशुभ
- बर - ऊपर, पर
- बा - साथ, अनुसार
- बिल (अरबी) - साथ, से, में
- विला (अरबी) - बिना
- बे - बिना
- ला (अरबी) - बिना, निषेध, अभाव
- सर - मुख्य, श्रेष्ठ
- हम (संस्कृत सम से) - साथ, समान
- हर - प्रत्येक
नोट - उर्दू के सारे उपसर्ग अरबी-फ़ारसी से लिए गये हैं। ये संख्या में लगभग (19) हैं।
प्रत्यय
जो शब्दांश शब्दों के अंत में जुड़कर उनके अर्थ में विशेषता या परिवर्तन ला देते हैं, वे प्रत्यय कहलाते हैं, जैसे-
सुंदर + ता = सुंदरता
मनुष्य + त्व = मनुष्यत्व
प्यास + आ = प्यासा
प्रत्यय के प्रकार
प्रत्यय का भेद दो आधारों पर किया जा सकता हैं -
- कृत प्रत्यय
- तद्धित प्रत्यय
कृत प्रत्यय
वे प्रत्यय जो (क्रिया) के मूल रूप यानी धातु (root word) में जोड़े जाते हैं, कृत प्रत्यय कहलाते हैं। कृत् प्रत्यय से बने शब्द कृदन्त (कृत + अंत) शब्द कहलाते हैं। जैसे-
लिख + अक = लेखक
यहाँ अक कृत् प्रत्यय है तथा लेखक कृदंत शब्द है।
तद्धित प्रत्यय
वे प्रत्यय जो क्रिया के मूल रूप यानी धातु को छोड़कर अन्य शब्दों— (संज्ञा) सर्वनाम, विशेषण व अव्यय में जुड़ते हैं, तद्धित प्रत्यय कहलाते हैं । तद्धित प्रत्यय से बने शब्द तद्धितांत शब्द कहलाते हैं। जैसे—
सेठ + आनी = सेठानी
यहाँ आनी तद्धित प्रत्यय है तथा सेठानी तद्धितांत शब्द है।
इस प्रकार कृत् और तद्धित प्रत्यय में मूल अंतर यह है कि कृत् प्रत्यय धातुओं में लगते हैं, जबकि तद्धित प्रत्यय धातुभिन्न शब्दों में लगते हैं ।
दोनों प्रत्ययों में समानता यह है कि दोनों प्रकार के प्रत्ययों से बनने वाले शब्द संज्ञा या विशेषण होते हैं।
हिन्दी के प्रायः सभी कृत् एवं तद्धित प्रत्यय संस्कृत के कृत् एवं तद्धित प्रत्ययों से ही विकसित हुए हैं।
हिन्दी के कृत् प्रत्यय (Primary Suffixes)
हिन्दी के तद्धित प्रत्यय (Nominal Suffixes)
प्रत्ययों के पूर्वोक्त वर्गीकरण ( कृत् व तद्धित) को कई भाषाविद् उचित नहीं मानते हैं क्योंकि हिन्दी में कई प्रत्यय ऐसे हैं जो दोनों रूपों में आते हैं अर्थात् धातु में भी जुड़ते हैं और संज्ञा आदि शब्दों में भी जुड़ते हैं; जैसे
एरा
लुट + एरा (कृत् प्रत्यय) = लुटेरा
चाचा + एरा (तद्धित प्रत्यय) = चचेरा
आई
पढ़ + आई (कृत् प्रत्यय) = पढ़ाई
भला + आई (तद्धित प्रत्यय) = भलाई
नी
कतर + नी (कृत् प्रत्यय) = कतरनी
ऊंट + नी (तद्धित प्रत्यय) = ऊंटनी
ये भाषाविद् प्रत्ययों के वर्गीकरण के लिए ऐतिहासिक आधार को उचित ठहराते हैं ।
इतिहास या स्रोत के आधार पर हिन्दी प्रत्ययों को चार वर्गों में बाटा गया है -
- तत्सम प्रत्यय
- देशज प्रत्यय
- तद्भव प्रत्यय
- विदेशज प्रत्यय
तत्सम प्रत्यय
तद्भव प्रत्यय
देशज प्रत्यय
विदेशज प्रत्यय
अरबी-फ़ारसी प्रत्यय
अंग्रेज़ी प्रत्यय
अन्य लेख पढ़ें !
➭ वर्णमाला ➭ संज्ञा ➭ लिंग ➭ वचन ➭ कारक ➭ सर्वनाम ➭ विशेषण ➭ क्रिया ➭ क्रिया विशेषण ➭ संधि ➭ समास ➭ शब्दालंकार ➭ रस ➭ अर्थालंकार ➭ विराम चिन्ह ➭ क्रिया व क्रिया के भेद
➭ वर्णमाला ➭ संज्ञा ➭ लिंग ➭ वचन ➭ कारक ➭ सर्वनाम ➭ विशेषण ➭ क्रिया ➭ क्रिया विशेषण ➭ संधि ➭ समास ➭ शब्दालंकार ➭ रस ➭ अर्थालंकार ➭ विराम चिन्ह ➭ क्रिया व क्रिया के भेद

Join the conversation