संवेग व स्थायीभाव का अर्थ, परिभाषा व प्रकार | Emotion and Sentiment
मनुष्य अपनी रोजाना की जिन्दगी में सुख, दुःख, भय, क्रोध, प्रेम, ईर्ष्या, घृणा आदि का अनुभव करता है। वह ऐसा व्यवहार किसी उत्तेजनावश करता है।
संवेग व स्थायीभाव
संवेग का अर्थ व परिभाषा
मनुष्य अपनी रोजाना की जिन्दगी में सुख, दुःख, भय, क्रोध, प्रेम, ईर्ष्या, घृणा आदि का अनुभव करता है। वह ऐसा व्यवहार किसी उत्तेजनावश करता है। यह अवस्था संवेग कहलाती है। "संवेग" के लिए अंग्रेजी का शब्द है - इमोशन। इस शब्द की उत्पत्ति लेटिन भाषा के 'इमोवेयर' से हुई है, जिसका अर्थ है - 'उत्तेजित होना'।
इस प्रकार 'संवेग' को व्यक्ति की 'उत्तेजित दशा' कहते हैं। उदाहरणार्थ, जब हम भयभीत होते हैं, तब हम भय के कारण से बचने का उपाय सोचते हैं, हमारी बुद्धि काम नहीं करती है, हम भय की वस्तु से दूर भाग जाना चाहते हैं, हमारे सारे शरीर में पसीना आ जाता है, हम काँपने लगते हैं, और हमारा हृदय जोर से धड़कने लगता है।
हमारी इस उत्तेजित दशा का नाम ही संवेग है। इस दशा में हमारा बाह्य और आन्तरिक व्यवहार बदल जाता है। कुछ मुख्य संवेग हैं – सुख, दुःख, प्रेम, भय, क्रोध, आशा, निराशा, लज्जा, गर्व, ईर्ष्या, आश्चर्य और सहानुभूति।
'संवेग' के अर्थ को पूर्ण रूप से स्पष्ट करने के लिए कुछ परिभाषाएँ -
वुडवर्थ - "संवेग, व्यक्ति की उत्तेजित दशा है।"
क्रो व क्रो - “संवेग, गतिशील आन्तरिक समायोजन है, जो व्यक्ति के संतोष, सुरक्षा और कल्याण के लिए कार्य करता है।"
ड्रेवर – “संवेग, प्राणी की एक जटिल दशा है, जिसमें शारीरिक परिवर्तन प्रबल भावना के कारण उत्तेजित दशा और एक निश्चित प्रकार का व्यवहार करने की प्रवृत्ति निहित रहती है।"
किम्बल बंग – “संवेग, प्राणी की उत्तेजित मनोवैज्ञानिक और शारीरिक दशा है, जिसमें शारीरिक क्रियाएँ और शक्तिशाली भावनाएँ किसी निश्चित उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए स्पष्ट रूप से बढ़ जाती हैं।"
वैलेन्टीन – “रागात्मक प्रवृत्ति के वेग के बढ़ने को संवेग कहते हैं।"
इन परिभाषाओं से ये तथ्य स्पष्ट होते हैं
- संवेगावस्था में व्यक्ति असामान्य हो जाता है।
- संवेगावस्था में व्यक्ति में मनोवैज्ञानिक परिवर्तन होते हैं।
- संवेग मनोवैज्ञानिक कारणों से उत्पन्न होते हैं।
संवेग की विशेषताएँ
संवेगों के तीन पक्ष हैं - अनुभवात्मक, शारीरिक तथा व्यवहारात्मक। साहित्यकारों की रचना में अनुभवात्मक, शारीरिक स्थिति में परिवर्तन, एवं शारीरिक क्रिया के प्रति अनुक्रिया करना व्यवहारात्मक पक्ष है। ये सभी पक्ष संवेगों की इन विशेषताओं में प्रकट होते हैं। स्टाउट का कथन है - "प्रत्येक विशिष्ट प्रकार के संवेग में कुछ विचित्रता होती है, जिसकी परिभाषा नहीं की जा सकती है।"
संवेग की विचित्रता के कारण हम उसके स्वरूप को भली भाँति तभी समझ सकते हैं, जब हम उसकी विशेषताओं से पूर्णतया परिचित हो जायँ। अतः हम उसकी मुख्य विशेषताएँ प्रस्तुत कर रहे हैं,
तीव्रता
संवेग में तीव्रता पाई जाती है और वह व्यक्ति में एक प्रकार का तूफार उत्पन्न कर देता है। पर इस तीव्रता की मात्रा में अन्तर होता है, उदाहरणार्थ, अशिक्षित व्यक्ति की अपेक्षा शिक्षित व्यक्ति में, जो अपने संवेग पर नियन्त्रण करना सीख जाता है, संवेग की तीव्रता कम होती है। इसी प्रकार, बालकों की अपेक्षा वयस्कों में और स्त्रियों की अपेक्षा पुरुषों में संवेग की तीव्रता कम पाई जाती है।
व्यापकता
स्टायन के अनुसार - "निम्नतर प्राणियों से लेकर उच्चतर प्राणियों तक एक ही प्रकार के संवेग पाये जाते हैं।" इस कथन से स्पष्ट हो जाता है कि संवेग में व्यापकता होती है और वह सब प्राणियों में समान रूप से पाया जाता है, उदाहरणार्थ, बिल्ली को उसके बच्चों को छेड़ने से, बालक को उसका खिलौना छीनने से, और मनुष्य को उसकी आलोचना करने से क्रोध आ जाता है।
वैयक्तिकता
संवेग में व्यक्तिकता होती है, अर्थात् विभिन्न व्यक्ति एक ही संवेग के प्रति विभिन्न प्रतिक्रिया करते हैं, उदाहरणार्थ, भूखे भिखारी को देखकर एक व्यक्ति दया से द्रवित हो जाता है, दूसरा उसे भोजन देता है, और तीसरा, उसे ढोंगी कहकर भगा देता है।
संवेगात्मक मनोदशा
स्टाउट का कथन है - "एक निश्चित संवेग उसके समरूप संवेगात्मक मनोदशा का निर्माण करता है।" इस मनोदशा के कारण व्यक्ति उसी प्रकार का व्यवहार करता है, जैसा कि उसके साथ किया गया है, उदाहरणार्थ, यदि गृह-स्वामिनी किसी कारण से क्रुद्ध होकर रसोइये को डॉटती है, तो रसोइया अपने क्रोध को नौकरानी पर उतारता है।
संवेगात्मक सम्बन्ध
स्टाउट ने लिखा है - "संवेग का अनुभव किसी निश्चित वस्तु के सम्बन्ध में ही किया जाता है।" इसका अभिप्राय है कि संवेग की दशा में हमारा किसी व्यक्ति, या वस्तु, या विचार से सम्बन्ध होता है, उदाहरणार्थ, हमें किसी व्यक्ति, वस्तु, विचार या कार्य के प्रति ही क्रोध आता है। इनके अभाव में क्रोध के संवेग का उत्पन्न होना असम्भव है।
स्थानान्तरण
ड्रमण्ड व मैलोन का मत है - "संवेगात्मक जीवन में स्थानान्तरण का नियम एक वास्तविक तथ्य है।"
सुख या दुःख की भावना
स्टाउट के अनुसार - "अपनी विशिष्ट भावना के अलावा संवेग में निस्सन्देह रूप से सुख या दुःख की भावना होती है।" उदाहरणार्थ, हमें आशा में सुख का और निराशा में दुःख का अनुभव होता है।
विचार शक्ति का लोप
संवेग हमारी विचार का लोप कर देता है। अतः हम उचित या अनुचित का विचार किये बिना कुछ भी कर बैठते हैं, उदाहरणार्थ, क्रोध के आवेश में मनुष्य हत्या तक कर डालता है।
पराश्रयी रूप
स्टाउट के शब्दों में - “संवेग की एक विशेषता को हम इसका पराश्रयी रूप कह सकते हैं।" इसका अभिप्राय है कि पशु या व्यक्ति में जिस संवेग की अभिव्यक्ति होती है उसका आधार कोई विशेष प्रवृत्ति होती है, उदाहरणार्थ, अपनी प्रेमिका के पास अपने प्रतिद्वन्द्वी को देखकर प्रेमी को क्रोध आने का कारण उसमें काम प्रवृत्ति की पूर्व उपस्थिति है।
स्थिरता की प्रवृत्ति
संवेग में साधारणतः स्थिरता की प्रवृत्ति होती है, उदाहरणार्थ, दफ्तर में डाँट खाकर लौटने वाला क्लर्क अपने बच्चों को डाँटता या पीटता है।
क्रिया की प्रवृत्ति
स्टाउट का विचार है - "संवेग में एक निश्चित दिशा में क्रिया की प्रवृत्ति होती है।"
क्रिया की इस प्रवृत्ति के कारण व्यक्ति कुछ न कुछ अवश्य करता है, उदाहरणार्थ, लज्जा का अनुभव करने पर बालिका नीचे की ओर देखने लगती है या अपने मुख को छिपाने का प्रयत्न करती है।
व्यवहार में परिवर्तन
रेबर्न का मत है - "संवेग के समय व्यक्ति के व्यवहार के सम्पूर्ण स्वरूप में परिवर्तन हो जाता है।" उदाहरणार्थ, दया से ओतप्रोत व्यक्ति का व्यवहार उसके सामान्य व्यवहार से बिल्कुल बिन्नी होता है।
मानसिक दशा में परिवर्तन
संवेग के समय व्यक्ति की मानसिक दशा में अग्रलिखित क्रम में परिवर्तन होते हैं
- किसी वस्तु या स्थिति का ज्ञान, स्मरण या कल्पना।
- ज्ञान के कारण सुख या दुःख की अनुभूति।
- अनुभूति के कारण उत्तेजना।
- उत्तेजना के कारण कार्य करने की प्रवृत्ति ।
आन्तरिक शारीरिक परिवर्तन
- हृदय की धड़कन और रक्त का संचार बढ़ना।
- भय और क्रोध के समय पेट में पाचक रस का निकलना बन्द होना।
- भय और क्रोध के समय भोजन की सम्पूर्ण आन्तरिक प्रक्रिया का बन्द होना।
बाह्य शारीरिक परिवर्तन
- भय के समय काँपना, रोंगटे खड़े होना, मुख सूख जाना, घिग्घी बँधना।
- क्रोध के समय मुँह लाल होना, पसीना आना, आवाज का कर्कश होना, ओठों और भुजाओं का फड़कना।
- प्रसन्नता के समय हँसना, मुस्कराना, चेहरे का खिल जाना।
- असीम दुःख या आश्चर्य के समय आँखों का खुला रह जाना।
संवेगों के प्रकार (Kinds of Emotion)
संवेगों का सम्बन्ध मूलप्रवृत्तियों से होता है। चौदह मूलप्रवृत्तियों के चौदह ही संवेग हैं जो इस प्रकार हैं-
- भय
- क्रोध
- घृणा
- वात्सल्य
- करुणा व दुःख
- कामुकता
- आश्चर्य
- आत्महीनता
- आत्माभिमान
- एकाकीपन
- भूख
- अधिकार भावना
- कतिभाव
- आमोद
संवेगों का शिक्षा में महत्व
शिक्षा में संवेगों के महत्व की व्याख्या करते हुए रॉस ने लिखा है - शिक्षा के आधुनिक मनोविज्ञान में संवेगों का प्रमुख स्थान है और शिक्षण विधि में जो प्रगति आजकल हो रही है, उसका कारण सम्भवतः किसी अन्य तथ्य की अपेक्षा यह अधिक है। संवेग हमारे सब कार्यों को गति प्रदान करते हैं और शिक्षक को उन पर ध्यान देना अति आवश्यक है। शिक्षक, बालकों के संवेगों के प्रति ध्यान देकर उनका क्या हित कर सकता है,
इस पर हम निम्नांकित पंक्तियों में प्रकाश डाल रहे हैं-
- शिक्षक, बालकों के संवेगों को जाग्रत करके, पाठ में उनकी रुचि उत्पन्न कर सकता है।
- शिक्षक, बालकों को अपने संवेगों पर नियन्त्रण करने की विधियाँ बताकर, उनको शिष्ट और सभ्य बना सकता है।
- शिक्षक, बालकों के संवेगों का ज्ञान प्राप्त करके, उपयुक्त पाठ्यक्रम का निर्माण करने में सफलता प्राप्त कर सकता है।
- शिक्षक, बालकों में उचित संवेगों का विकास करके, उनमें उत्तम विचारों, आदर्शी, गुणों और रुचियों का निर्माण कर सकता है।
- शिक्षक, बालकों के भय, क्रोध आदि अवांछित संवेगों का मार्गान्तीकरण करके, उनको अच्छे कार्य करने के लिए प्रेरित कर सकता है।
- झा के अनुसार शिक्षक, बालकों के संवेगों को परिष्कृत करके उनको समाज के अनुकूल व्यवहार करने की क्षमता प्रदान कर सकता है।
- ब्लेयर तथा अन्य के अनुसार शिक्षक, बालकों में उपयुक्त संवेगों को जाग्रत करके, उनको महान कार्यों को करने की प्रेरणा दे सकता है।
- झा के अनुसार शिक्षक, बालकों की मानसिक शक्तियों के मार्ग को प्रशस्त करके, उन्हें अपने अध्ययन में अधिक क्रियाशील बनने की प्रेरणा प्रदान कर सकते हैं।
- रॉस के अनुसार शिक्षक, बालकों में वांछनीय संवेगों का विकास करके, उनमें कला, संगीत, साहित्य और अन्य सुन्दर वस्तुओं के प्रति प्रेम उत्पन्न कर सकता है।
- रॉस के अनुसार शिक्षक, बालकों में उपयुक्त संवेगों को जाग्रत करके, अपने शिक्षण को सफल बना सकता है, उदाहरणार्थ वह अपने गणित के शिक्षण को तभी सफल बना सकता है, जब वह बालकों में आश्चर्य का संवेग उत्पन्न कर दे।
सार रूप में, हम कह सकते हैं कि संवेग के अभाव में मानव मस्तिष्क अपनी किसी भी शक्ति को समाप्त करने में असमर्थ रहता है। अतः शिक्षक का यह प्रमुख कर्त्तव्य है कि बालकों मे उचित संवेगों का निर्माण और विकास करे। बी. एन. झा का यह कथन अक्षरशः सत्य है - “बालकों में संवेगों को जाग्रत करने का शिक्षक का कार्य बहुत महत्वपूर्ण है।"
स्थायीभाव का अर्थ व परिभाषा
मैक्डुगल के अनुसार 'व्यक्ति अनेक मूलप्रवृत्तियाँ लेकर संसार में आता है। इन मूलप्रवृत्तियों का सम्बन्ध विभिन्न प्रकार के संवेगों से होता है। ये संवेग ही स्थायी भाव का निर्माण करते हैं, उदाहरणार्थ, माँ में अपने बच्चों के प्रति दया, गर्व, आनन्द, सहानुभूति, वात्सल्य आदि के संवेग होते हैं।'
इन्हीं संवेगों के फलस्वरूप उसमें प्रेम के स्थायीभाव का निर्माण होता है। स्थायीभाव व्यक्ति के अतिरिक्त, किसी वस्तु, आदर्श, विचार, स्थान आदि के प्रति भी होता है, जैसे - बालक में अपने खिलौने के प्रति प्रेम का स्थायीभाव, चरित्रवान व्यक्ति में श्रेष्ठ आदर्शों या विचारों के प्रति सम्मान का स्थायीभाव, भारतीय में स्वदेश-प्रेम का स्थायीभावं। इस प्रकार, हम कह सकते हैं कि स्थायीभाव किसी व्यक्ति, वस्तु, विचार, आदर्श स्थान आदि के प्रति संवेगों का अर्जित और स्थायी रूप है।
“स्थायीभाव" के अर्थ को और अधिक स्पष्ट करने के लिए हम कुछ परिभाषाएँ दे रहेहैं,
1. रॉस - "स्थायीभाव मानसिक ढाँचे में अर्जित प्रवृत्तियों का संगठन है। "
2. रैक्स व नाइट – “स्थायीभाव किसी वस्तु के प्रति अर्जित संवेगात्मक प्रवृत्ति या ऐसी प्रवृत्तियों का संगठन है।"
3. वेलेन्टाइन – “स्थायीभाव किसी वस्तु या व्यक्ति के प्रति संवेगात्मक प्रवृत्तियों और भावनाओं का बहुत कुछ स्थायी और संगठित स्वरूप है।"
4. नन – “स्थायीभाव, भावना की एकाकी दशा नहीं है, वरन् भावनाओं का संगठन है, जो किसी वस्तु विशेष के सम्बन्ध में संगठित होती हैं और जिनमें स्थायित्व की पर्याप्त मात्रा होती है।"
स्थायीभावों के स्वरूप
साधारण स्थायीभाव
इस स्थायीभाव में किसी के प्रति केवल एक भावना या संवेग होता है, जैसे - बालिका में अपनी गुड़ियों के प्रति प्रेम का स्थायीभाव या बालक में कठोर शिक्षक के प्रति भय का स्थायीभाव होता है।
जटिल स्थायीभाव
इस स्थायीभाव में एक से अधिक भावनाएँ या संवेग होते हैं, जैसे- बालक में कठोर शिक्षक के प्रति घृणा का स्थायीभाव होता है। यदि शिक्षक उसे छोटी-छोटी बातों पर दण्ड देता है, तो उसे शिक्षक पर क्रोध आता है। धीरे धीरे उसे शिक्षक से अरुचि हो जाती है। सम्भवतः वह उससे प्रतिशोध लेने की भावना भी रखने लगता है। फलस्वरूप, उसमें शिक्षक के प्रति घृणा उत्पन्न हो जाती है। यह घृणा एक जटिल स्थायीभाव है, जिसका निर्माण- भय, क्रोध, अरुचि और प्रतिशोध के संवेगों और भावनाओं से हुआ है।
मूर्त स्थायीभाव
इस स्थायीभाव का सम्बन्ध किसी मूर्त या स्थूल वस्तु से होता है, जैसे - व्यक्ति, पशु, पुस्तक, निवास स्थान आदि ।
अमूर्त स्थायीभाव
इस स्थायीभाव का सम्बन्ध अमूर्त या सूक्ष्म वस्तुओं से होता है, जैसे - भक्ति, विचार, सत्य, आदर्श, अहिंसा, सम्मान, स्वच्छता, देश प्रेम आदि।
नैतिक स्थायीभाव
यह स्थायीभाव नैतिक चरित्र का वास्तविक अंग है और साधारणतः परम्परागत होता है, जैसे - न्याय या सत्य के प्रति प्रेम, क्रूरता या बेईमानी के प्रति घृणा।
स्थायीभावों की विशेषताएँ
स्थायीभाव, मानव द्वारा अर्जित व्यवहार परिवर्तन है। इस व्यवहार परिवर्तन का मुख्य कारण है - संवेगों तथा मूलप्रवृत्तियों में शोधन तथा प्रशिक्षण इसलिये स्थायीभावों की विशेषताओं को इस प्रकार समझा जा सकता है तथा प्रशिक्षण इसलिए स्थायीभावों की-
- स्थायीभाव, जन्मजात न होकर अर्जित होते हैं।
- स्थायीभाव, मानसिक प्रक्रिया न होकर, मानसिक रचना होते हैं।
- स्थायीभाव मूर्त और अमूर्त - दोनों प्रकार की वस्तुओं के प्रति होते हैं, अर्थात् - व्यक्ति, वस्तु, गुण, अवगुण, आदर्श, विचार, स्थान आदि किसी के प्रति हो सकते हैं।
- स्थायीभाव, व्यक्ति के चरित्र और व्यक्तित्व के आधार होते हैं।
- स्थायीभाव, व्यक्ति के व्यवहार को प्रेरित और नियन्त्रित करते हैं।
- स्थायीभावों का निर्माण साधारणतः एक से अधिक संवेग से होता है।
- स्थायीभावों में विचारों, इच्छाओं, भावनाओं और अनुभवों का समावेश रहता है।
- जलोटा के अनुसार स्थायीभाव, मानसिक रचना के अंग होने के कारण हममें सदैव विद्यमान रहते हैं।
- स्टर्ट तथा ओकडन के अनुसार स्थायीभाव में मानव अनुभवों के साथ-साथ परिवर्तन होते रहते हैं।
स्थायीभावों का शिक्षा में महत्व
शिक्षा में स्थायीभावों के महत्व का वर्णन करते हुए, स्टर्ट तथा ओकडन ने लिखा है - “स्थायीभाव हमारे जीवन में अत्यधिक महत्वपूर्ण कार्य करते हैं। वे मानसिक और संवेगात्मक संगठन की इकाइयाँ हैं एवं तुलनात्मक रूप में स्थायी होते हैं। अतः शैक्षिक दृष्टिकोण से स्थायीभाव बहुत महत्वपूर्ण हैं।"
शैक्षिक दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण होने के कारण बालकों में अच्छे स्थायीभावों का निर्माण करना शिक्षक का सर्वप्रथम कर्तव्य हो जाता है। वह ऐसा किस प्रकार कर सकता है और इससे बालकों को क्या लाभ हो सकता है, इस पर हम नीचे की पंक्तियों में दृष्टिपात कर रहे हैं
- शिक्षक, बालकों को अपने देश के महान् वीरों की कहानियाँ सुनाकर उनमें देश प्रेम के स्थायीभाव का निर्माण कर सकता है।
- शिक्षक, बालकों में नैतिक स्थायीभावों का विकास करके, उनमें नैतिक गुणों का विकास कर सकता है और इस प्रकार उनके नैतिक उत्थान में योग दे सकता है।
- शिक्षक, बालकों में घृणा के स्थायीभाव को प्रबल बनाकर, उनमें हिंसा, असत्य, बेईमानी आदि दुर्गुणों से संघर्ष करने की क्षमता उत्पन्न कर सकता है।
- शिक्षक, बालकों में प्रेम का स्थायीभाव उत्पन्न करके, उनकी खेल, कविता, संगीत, साहित्य आदि में विशेष रुचि जाग्रत कर सकता है। इस प्रकार, वह उनके व्यक्तित्व के विकास में सहायता दे सकता है।
- रॉस के अनुसार शिक्षक बालकों में आत्म-सम्मान का स्थायीभाव विकसित करके, उनके मानसिक जीवन को एकता प्रदान कर सकता है।
- रॉस के अनुसार - स्थायीभाव, आदर्शों का निर्माण करके चरित्र के निर्माण में सहायता देते हैं। अतः शिक्षक को बालकों में उत्तम स्थायीभावों का निर्माण करना चाहिए।
- मैक्डूगल के अनुसार - आत्म-सम्मान का स्थायीभाव, चरित्र और यह नैतिक स्थायीभावों में सर्वश्रेष्ठ है। अतः शिक्षक को बालकों में इस स्थायीभाव को पूर्ण रूप से विकसित करना चाहिए।
- शिक्षक को बालकों में अच्छे स्थायीभावों का निर्माण करने के लिए अग्रलिखित कार्य करने चाहिए - (1) उच्च आदर्शों और लक्ष्यों के लिए प्रेरणा देना, (2) महान व्यक्तियों के विचारों और आदर्शों से परिचित कराना, (3) प्रसिद्ध वैज्ञानिकों, श्रेष्ठ साहित्यकारों आदि की जीवनियाँ सुनाना, (4) कार्य और सिद्धान्त के उत्तम उदाहरण प्रस्तुत करना आदि।
अन्त में, हम स्टर्ट व ओकडन के शब्दों में कह सकते हैं - "इस बात की ओर ध्यान देना शिक्षा का एक महत्वपूर्ण कार्य होना चाहिए कि बालक द्वारा जिन स्थायीभावों का निर्माण किया जाय, वे समाज की आवश्यकताओं के अनुकूल हों।"
स्थायीभावों को विकसित करना शिक्षा का प्रमुख कार्य है। इनसे नई पीढ़ी में भविष्य के प्रति आदर्शों का निर्माण होता है। मानसिक बोध तथा संवेगों के संगठन से स्थायीभावों का विकास सम्भव है।

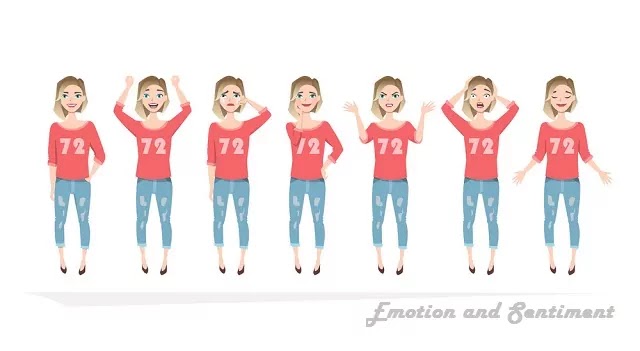
Join the conversation